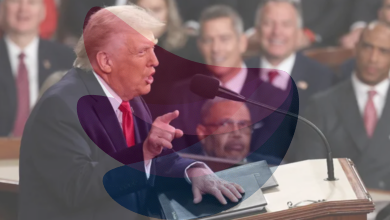नेपाल का चीन को नोट-प्रिंटिंग ठेका: क्या यह बीजिंग की करेंसी-डिप्लोमैसी का हिस्सा है या काठमांडू की रणनीतिक मजबूरी?

नेपाल का भारत से हटकर चीन को मुद्रा छपवाने का निर्णय सिर्फ एक प्रशासनिक या तकनीकी बदलाव नहीं है, बल्कि यह दक्षिण एशिया की भू-राजनीतिक शक्ति-संतुलन में उभरते नए समीकरणों का हिस्सा है। इस निर्णय के तीन बड़े आयाम हैं — आर्थिक, रणनीतिक और कूटनीतिक।
पहला आयाम आर्थिक लाभ से जुड़ा है। चीन दुनिया के उन कुछ देशों में है, जिनके पास बड़े पैमाने पर अत्याधुनिक करेंसी प्रिंटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है। कम लागत, तेज़ उत्पादन, आधुनिक सुरक्षा फीचर्स — ये सभी लाभ चीन को प्रतिस्पर्धी बनाते हैं। नेपाल जैसा छोटा देश, जिसका बजट सीमित है, सस्ते विकल्प को प्राथमिकता देगा, यह स्वाभाविक है। चीन इस क्षेत्र में कम कीमत के साथ उच्च गुणवत्ता भी देता है।
दूसरा आयाम तकनीकी श्रेष्ठता से जुड़ा है। चाइना बैंकनोट प्रिंटिंग एंड मिंटिंग कॉरपोरेशन दुनिया की उन कंपनियों में से एक है, जो होलोग्राफिक सुरक्षा पैटर्न, माइक्रो-टेक्स्टिंग, उन्नत वॉटरमार्क और एंटी-काउंटरफिटिंग तकनीक में लगातार निवेश करती हैं। नेपाल ने देखा कि चीन इन तकनीकी मानकों पर भारत से अधिक प्रतिस्पर्धी है, इसलिए उसने दीर्घकालिक दृष्टि से यह बदलाव स्वीकार किया।
तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण आयाम कूटनीतिक प्रभाव है। नेपाल का यह निर्णय 2015 में भारत द्वारा जताई गई आपत्तियों से उत्पन्न कूटनीतिक संवेदनशीलताओं से जुड़ा है। कुछ नोटों के राजनीतिक नक्शों के कारण भारत ने अपनी नाराज़गी प्रकट की थी। नेपाल, जो अपनी संप्रभुता पर बहुत संवेदनशील है, ने इसे अपनी स्वतंत्रता में हस्तक्षेप के रूप में लिया। ऐसे में चीन ने बिना किसी कूटनीतिक दबाव के प्रस्ताव स्वीकार कर नेपाल को विकल्प दिया।
यह निर्णय दक्षिण एशिया में चीन की बढ़ती आर्थिक उपस्थिति का हिस्सा है। नेपाल को निवेश, व्यापार और इंफ्रास्ट्रक्चर सहायता देना चीन की “बेल्ट एंड रोड” रणनीति का ही विस्तार है। करेंसी प्रिंटिंग जैसे संवेदनशील क्षेत्र में प्रवेश चीन को नेपाल की आर्थिक-प्रशासनिक संरचनाओं तक पहुंच दिलाता है।
भारत के लिए यह एक रणनीतिक चेतावनी है। नेपाल, जिसके साथ भारत के सांस्कृतिक और ऐतिहासिक संबंध गहरे हैं, अब चीन को तीव्र गति से स्वीकार कर रहा है। भारत को अपने पड़ोस में प्रभाव बनाए रखने के लिए न सिर्फ आर्थिक सहयोग, बल्कि भावनात्मक और कूटनीतिक साझेदारी को भी मजबूत करना होगा।
यह निर्णय भले ही तकनीकी दिखता हो, लेकिन इसके लहरदार प्रभाव लंबे और गहरे हैं।